इस पोस्ट के माध्यम से आप काव्य-हेतु क्या है ? भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने कितनें काव्य हेतु मानें हैं ? और उनकी क्या परिभाषा दी है ? आदि प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे।
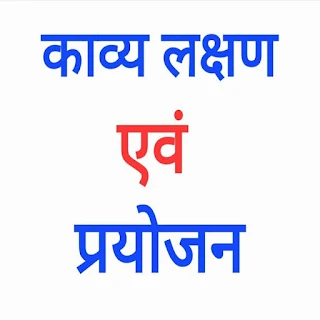 |
| काव्य हेतु लक्षण एवं प्रयोजन । शिक्षा विचार । Kavya Hetu Lakshan Evam Prayojan । Shiksha Vichar |
काव्य हेतु
- विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे कारण न हो अर्थात् कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। जब प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में अवश्य ही कोई न कोई कारण होता है तो फिर साहित्य में कारण का अभाव क्यों ? साहित्य को जीवन की अभिव्यक्ति माना गया है। अतः जिस वस्तु का जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध है। उसके आरंभ में कारण न हो यह असंभव है।
- काव्य अथवा साहित्य के कारणों को विभिन्न नामों से पुकारा गया है आज कारण के लिए हेतु शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है और अब यह रुढ़ भी हो चुका है। अतः हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य-हेतु क्या है ? इस विषय पर अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने गहन चिंतन एवं मनन किया है। यद्यपि इस विषय पर समस्त विद्वान एकमत नहीं है फिर भी अधिकांश विद्वान प्रकारांतर से एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हुए दिखाई देते हैं
- भारतीय काव्यशास्त्रियों में जिन्होंने काव्य-हेतुओं क निरूपण किया। उनमें दण्डी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट आदि आचार्यों का योगदान उल्लेखनीय है। इन सभी आचार्यों ने शब्द-भेद से शक्ति अर्थात् प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को कवि-कर्म के लिए आवश्यक तत्व माना है।
- दण्डी ने तीन काव्य-हेतु बताए हैं- नैसर्गिक, प्रतिभा, निर्मल शास्त्रज्ञान और अभ्यास।
- रुद्रट एंव कुंतक ने भी इनकी संख्या तीन गिनाई है- शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास।
- वामन ने तीन प्रकार के काव्य-हेतु माने है- लोक(लोक व्यवहार ज्ञान), विद्या(विभिन्न शास्त्रज्ञान), प्रकीर्ण
- प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने छ: हेतुओं को गिना है- लक्ष्य तत्व(अन्य काव्यानुशीलन), अभियोग(अभ्यास), वृद्ध सेवा(गुरु चरणों में बैठकर), अवेक्षण(उपयुक्त शब्दों का चुनाव), प्रतिमान(प्रतिभा) और अवधान(चित्त की एकाग्रता)।
आचार्य मम्मट के सम्मुख ये सभी काव्य-हेतु थे। अतः उन्होंने इनका अध्ययन करने के पश्चात् इन सब को तीन काव्य-हेतुओं में अंतर्भूत कर दिया-
शक्तिर्निपुणता लोके काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात्।
काव्यशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुभ्वे।।
- शक्तिनिपुणता अर्थात् (1)शक्ति (कवित्व का बीजरूप संस्कार) जिस के बिना काव्य-रचना नहीं हो सकती और यदि होती है तो वह हास्यास्पद बन जाती है, (2)लोकशास्त्र अर्थात् काव्य आदि के निरीक्षण तथा ज्ञान से उत्पन्न योग्यता एंव निपुणता और (3)काव्य जानने वाली शिक्षा द्वारा प्राप्त अभ्यास- ये काव्य-सृजन के हेतु माने गए हैं।
आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत 'शक्ति', दण्डी और वामन द्वारा स्वीकृत प्रतिभा का ही दूसरा नाम है।
- मम्मट की निपुणता के अंतर्गत दण्डी-सम्मत निर्मल शास्त्रज्ञान, रुद्रट-सम्मत व्युत्पत्ति और वामन-सम्मत लोक, विद्या, लक्ष्य-तत्व और अवेक्षण का समावेश हो जाता है और इनके अभ्यास के अंतर्गत दण्डी तथा वामन द्वारा स्वीकृत अभियोग तथा वामन द्वारा प्रस्तुत वृद्ध-सेवा आ जाते हैं। वामन प्रस्तुत 'अवधान' भी अपनी विशिष्ट महत्ता रखता है, परंतु यह काव्य का अलग हेतु न होकर निपुणता और अभ्यास के अंतर्गत आ जाता है। अब इस शंका का समाधान कर लेना भी समुचित होगा कि इन तीन काव्य-हेतुओं में से कौन-सा हेतु श्रेष्ठ है और शेष दो की क्या स्थिति है ?
प्रतिभा
- जहां तक प्रतिभा का प्रश्न है, यह काव्य का अनिवार्य एंव सर्वोत्कृष्ट हेतु है। इसकी महत्ता तो इसी बात से स्पष्ट है कि सभी विद्वानों इसे किसी-न-किसी रूप में स्वीकार किया है। अंग्रेजी में तो यहां तक कहा गया है कि
"Poets are born, not made"
- संस्कृत साहित्यशी में भामह से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक प्राय: सभी प्रमुख कवियों ने प्रतिभा का लक्षण प्रस्तुत किया है और इसे अनिवार्य सर्वोत्कृष्ट काव्य-हेतु के रूप में स्वीकार किया है।
- प्रतिभा का लक्षण बताने वाले उल्लेखनीय आचार्यों में सर्वप्रथम भामह का नाम सामने आता है। भामह ने काव्य-रचना में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित करते हुए कहा है-
गुरुदेशादध्येतुं शास्त्रं जङधिमोडप्यलम्।
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः।।
- अर्थात् शास्त्र पढ़ने और काव्य-निर्माण करने में बहुत अंतर है। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़-बुद्धि के लिए भी संभव हो सकता है, पर काव्य-निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है।
- भामह के पश्चात वामन ने प्रतिभा को 'प्रकीर्ण' के अंतर्गत गिनाकर उसे प्रमुख स्थान न देते हुए भी 'कविता-बीज' मान कर प्रकारांतर से उसकी महत्ता दिखाई है।
- रुद्रट ने काव्य-रचना के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को आवश्यक मानते हुए प्रतिभा को ही मुख्य माना है। उनके अनुसार प्रतिभा होने पर सहृदय के अंतर में अनेक प्रकार के वाक्य अनायास ही प्रस्फुटित होते हैं-
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधयेस्य।
अक्लिष्टानि पदानि च विभांति यस्यामसौ शक्ति:।।
अर्थात् जिसके बल पर कवि अपने एकाग्र (Concentrated) मन में विस्फुरित विभिन्न अभिधेयों को अनुकूल शब्द में अनायास अभिव्यक्त करता जाता है, उसे शक्ति या प्रतिभा कहते हैं।
रुद्रट ने काव्य के कारण रूपी शक्ति या प्रतिभा को दो भेदों में देखा है- (1)सहजा (2)उत्पाद्य।
- 1. सहजा- सहजा इश्वर-प्रदत और पूर्व संस्कारो द्वारा संचित जन्मजात शक्ति है।
- 2. उत्पाद्य- अध्ययन, अभ्यास और सत्संग से प्राप्त होती है। रुद्रट ने इन दोनों में सहजा को मुख्यता दी है।
आचार्य दण्डी ने प्रतिभा की मुख्यता को स्वीकार न करते हुए अपना मत 'काव्यदर्श' में इस प्रकार व्यक्त किया है-
न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधि प्रतिभानद्भुम्।
श्रु तेन यत्नेन च वागुपासित ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्।।
अर्थात् यदि किसी व्यक्ति में पूर्व-वासनाजन्य शक्ति या प्रतिभा न भी हो तब भी वाग्देवी किसी-किसी व्यक्ति पर शास्त्र और अभ्यास से कृपा कर ही देती हैं।
वामन के अनुसार केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास उस व्यक्ति को कवि नहीं बना सकते, जिसके भीतर प्रतिभा का बीज है ही नहीं। इसी बात की पुष्टि करते हुए आचार्य वामन कहते हैं-
शक्ति कवित्य बीजरूपा, यां बिना काव्यं न प्रसरेत,
प्रसंत वा उपहासनीय स्यात्।
अर्थात् शक्ति के बिना काव्य का निर्माण हो सकता है परंतु वह काव्य का उपहासमात्र होगा अर्थात प्रतिभा ही कवित्व का कारण है।
भट्टतौत ने भी नए-नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा की संज्ञा से अभिहित किया है-
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता।
भट्टतौत के लक्षण में केवल आतंरिक रूप की चर्चा ललित शब्दावली में की गई है। इन सब के विपरित कुंतक और मम्मट का लक्षण प्रतिभा के कारण पर विशिष्ट प्रकाश डालता है।
प्राक्तनाद्यतनसंस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कविशक्ति:।
अर्थात् पूर्वजन्म तथा इस जन्म के संस्कार के परिपाक से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व-शक्ति प्रतिभा कहलाती है।
इसी प्रकार मम्मट ने भी 'शक्ति: कवित्व बीजरूपा: संस्कार विशेष:' कहकर प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है।
हमें You Tube पर Subscribe करें
- आनंदवर्द्धन ने प्रतिभा को अनिवार्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। उनके कथनानुसार कवि का अशक्तिजन्य दोष तुरंत और अनायास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है, कवि के अव्युत्पत्तिजन्य दोष को उसकी प्रतिभा आच्छादित कर देती है-
अव्युत्पत्ति कृतो दोष: शक्त्या संव्रियते कवे:
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य भगित्येवाव भासते।।
- दूसरे शब्दों में व्युत्पत्ति में अशक्तिजन्य दोष को आच्छादित करने की क्षमता नहीं है। अत: शक्ति अनिवार्य हेतु किंतु व्युत्पत्ति अनिवार्य न होते हुए भी वांछित हेतु अवश्य है। प्रतिभा को अनिवार्य इसलिए माना गया है क्योंकि यदि कवि में यह विद्यमान है तो कवि अनेक प्रकर की कल्पनाएं कर उन को काव्य रूप दे सकता है और इस प्रकार नवीन विषयों का उत्पादन निरंतर होता रहता है। आनंदवर्द्धन के इस विवेचन की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों के समन्वित रूप को ही काव्य-हेतु माना है और तीनों के पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया।
इनकी तरह मम्मट ने भी तीनों अर्थात् शक्ति, निपुणता और अभ्यास को समान सा ही महत्व दिया है। इसीलिए उन्होंने तीनों को मिलाकर एक वचन हेतु कहा है-
'हेतुर्नतु हेतव:'
इस प्रकार काव्य-हेतु-विषयक विवेचन से सिद्ध होता है कि मम्मट के उपरांत इस विवेचन की दिशा ही बदल गई।
- वाग्भट प्रथम ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का हूतु माना है, लोक और शास्त्रज्ञान से उत्पन्न हुई संस्कार विशेष व्युत्पत्ति को उसका भूषण माना और अभ्यास को सामान्य रूप से एक ग्राह्य तत्व अर्थात् अभ्यास उसकी उत्पत्ति का वर्धक है, माना है।
- आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा के रूद्रट-सम्मत उत्पाद्या (अर्थात् व्युत्पत्तिजन्य) नामक एक भेद से अथवा राजशेखर द्वारा प्रस्तुत प्रतिभा की सर्वोत्कृष्टता से प्रेरणा प्राप्त कर प्रतिभा आदि तीन हेतुओं में से केवल प्रतिभा को, उस प्रतिभा को, जिसका व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा पोषण होता है, काव्य हेतु माना-
प्रतिभास्य हेतु:। व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां संस्कार्य।।
अर्थात् प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के संस्कार अथवा परिष्कारक हेतु हैं। हेमचंद्र कए इस कथन को वाग्भट द्वितीय ने ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया।
- जयदेव पीयूष ने एक उदाहरण द्वारा इसका स्पष्टीकरण और अनुमोदक किया- जिस प्रकार मिट्टी और जल से युक्त बीज, लता की उत्पत्ति का हेतु है, उसकी व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त प्रतिभा काव्य का हेतु है।
- संस्कृत साहित्यशास्त्र के अंतिम महान् आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने भी 'रसगंगाधर' में काव्य का कारण केवल प्रतिभा को ही माना है और इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस शक्ति के द्वारा काव्य के अनुकूल शब्द और अर्थ कवि के मन में जल्दी आते हैं उसे प्रतिभा कहते हैं। हेमचंद्र के समान उन्होंने भी व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का कारण स्वीकृत किया है, न कि काव्य का।
- इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि व्युत्पत्ति और अभ्यास कई परिस्थितियों में प्रतिभा के कारण नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने प्रतिभा को दो भागों में विभक्त किया है। पहली प्रारब्धवश जो किसी दिव्य या महापुरुषादि को प्राप्त होती है और दूसरी व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्राप्त।
अत: इन मतों से स्पष्ट है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में दण्डी ही एक ऐसे आचार्य हैं जो प्रतिभा के बिना भी कई अवस्थाओं में व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्योत्पत्ति को स्वीकृत करते हैं, जबकि अन्य आचार्य प्रतिभा को ही अनिवार्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं।
आधुनिक काल के हिंदी विद्वानों में 'आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी' ने प्रतिभा को महत्व देते हुए कहा है-
"कलाकार का मन भण्डार है जिसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां शब्द, विचार, चित्र, इकट्ठे होते रहते हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा में जबकि कवि-प्रतिभा के ताप से एक नया रसायन, एक चामत्कारिक योग उत्पन्न नहीं हो जाएगा।"
इधर डा० भगीरथ मिश्र अनुभूति के समय प्रतिभा के बारे में कहते हैं कि
"अपनी अनुभूति को प्रकट करने अथवा उसे दूसरों की अनुभूति में परिणत करने की विह्वलता का जब कवि अनुभव करता है, तभी प्रतिभा काव्य-रचना में प्रवृत्त होती है और व्युत्पत्ति और अभ्यास से काव्य का विकास होता है।"
- इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभा काव्य की मूल प्रेरक शक्ति है। जब कभी के अंतः करण में प्रेरणा का सहज स्फूरण होता है तब यह प्रतिभा-जन्य कल्पना से जिन सुरम्य भावों की सृष्टि करता है वे सहृदय संवेद्य होते हैं। प्रतिभा के बल पर ही वह उचित और अनुचित में निर्णय कर सकता है। अतः काव्य-सृजन में प्रतिभा का प्रमुख स्थान है।
- साहित्य आचार्यों के अतिरिक्त कवियों ने भी प्रतिभा की महत्ता को स्वीकार किया है। आधुनिक कवियों में जगन्नाथदास 'रत्नाकर', सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन 'पंत', महादेवी वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। जिन्होंने काव्य शक्ति में प्रतिभा को विशेष महत्व दिया है। महादेवी वर्मा के अनुसार "साहित्य सृजन केवल रूचि, विवशता या परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की भी आवश्यकता होती है।"
इसी प्रकार रीतिकालीन कवि श्री पति ने भी "शक्ति सुपुण्य विशेष है, जा बिन कवित्व न होत" कह कर प्रतिभा की महानता को स्वीकार किया है।
व्युत्पत्ति
- व्युत्पत्ति को 'काव्यप्रकाश' में निपुणता की संज्ञा से अभिहित किया गया है। इसकी प्राप्ति के दो कारण बतलाए गए हैं- लोक के निरीक्षण से और काव्य एवं शास्त्रों के अध्ययन से। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन से ईश्वर- प्रदत्त प्रतिभा का परिपोषण होता है। इससे प्रतिभा में प्रखरता आ जाती है और वह चमत्कृत, परिष्कृत, शक्ति- संपन्न और मर्मस्पर्शिनी हो उठती है। परंतु इससे प्रतिभा को अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती अन्यथा सभी शास्त्रज्ञ और लोक व्यवहार पटु व्यक्ति कविता करने की क्षमता रखते।
- इसी प्रकार दु:ख, शोक और विरहजन्य मानसिक क्लेशों या आघातों के कारण कभी-कभी सुप्त प्रतिभा जाग उठती है, परंतु ये मानसिक आघात प्रतिभा के उत्पादक-कारण न बनकर प्रेरणा-कारण माने जाएंगे। अत: हानि उठाए हुए व्यापारी, हारे हुए जुआरी, पुत्र-वियुक्त पिता व माता अथवा विधवाएं आदि सभी के सभी कवि-कर्म में जा जाएंगे।
डॉ० सत्यदेव चौधरी के कथनानुसार "वास्तव में प्रतिभा सहजा है, उत्पाद्या नहीं। अत: रुद्रट द्वारा प्रतिभा के उत्पाद्या नामक भेद से हम तभी सहमत हैं, जब इसका अर्थ 'जन्या' न होकर 'पोष्या' माना जाए।"
हेमचंद्र जी कहते हैं कि "व्युत्पत्ति पूर्व-विद्यमान प्रतिभा का संस्कार करती है, न कि उत्पादन।"
अभ्यास
- काव्य-सृजन का तीसरा काव्य-हेतु अभ्यास है। निपुणता की सफलता या सार्थकता अभ्यास पर निर्भर है। अभ्यास के द्वारा ही सुयोग्य शिष्य गुरु से प्राप्त शिक्षा को विकसित कर पाता है। परंतु कई विद्वानों ने न तो इसे काव्य का प्रमुख हेतु माना है, न अनिवार्य हेतु और न आवश्यक हेतु। क्योंकि ऐसे भी कवि संसार में हो चुके हैं, जिसकी प्रथम रचना ही उनकी अमर कृति बन गई है। उदाहरणार्थ-
महर्षि वाल्मीकि का 'मा निषाद प्रतिष्ठां स्वम्•••' यह प्रथम श्लोक ही इस तथ्य का प्रमाण है।
- चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' केवल तीन ही कहानियों से हिंदी कहानी-साहित्य में अपना नाम अमर कर गए। हां, अभ्यास से कवि-प्रतिभा में और उसके द्वारा तत्प्रणीत काव्य में परिष्कार अवश्य आ जाता है। अत: प्रतिभा के परिष्करण के लिए इस तत्व का ग्रहण नितांत आवश्यक है।
- जिस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य-हेतुओं पर विद्वानों में मतभेद रहा है, उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी यह विषय विद्वानों का मत-वैभिन्नय का कारण रहा है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य-हेतुओं का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया है। तथापि हम उनके द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत काव्य संबंधी विचारों से काव्य-हेतु का पता लगा सकते हैं। काव्य के विषय में बात करते हुए यूनानी आचार्य 'प्लेटो' सफल कलाकार के लिए प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण को आवश्यक मानते हैं।
- यूनान के महान आचार्य अरस्तू ने कार्य संबंधी विवेचन करते हुए सजगता, प्रतिभा, अभ्यास, चिंतन, कला-चमत्कार और अध्ययन कवि के लिए अनिवार्य गुण माने हैं।
- होरेस प्रतिभा, शास्त्र-ज्ञान, सजग विवेक और चिंतन को काव्य-हेतु मानते हुए प्रतिभा और शास्त्र-ज्ञान के समीकरण पर बल देते हैं।
- लोंजाइनस ने प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया परंतु उदात्त के विवेचन में ही कही गई पांच बातें इनमें ही समाहित हो जाती हैं। महान धारणाओं की क्षमता, विषय की गरिमा, भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार-योजना उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय में रचना-विधान।
- इसी प्रकार कार्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए अंग्रेजी कवि शैली ने भी प्रतिभा, चिंतन-मनन अभ्यास और अध्ययन का काव्य-हेतु के रूप में संकेत किया है। उन्होंने कवि के लिए यह आवश्यक माना है कि वह श्रेष्ठ परम बुद्धिमान एवं विश्रुत होना चाहिए। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने प्रतिभा, चिंतन-मनन, विवेक, अध्ययन और अभ्यास को काव्य हेतु माना है जो भारतीय प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में अंतर्भूत हो जाते हैं।
- अत: हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के विकास के लिए बीज, खाद और जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार काव्य-वृक्ष भी प्रतिभा रूपी बीज द्वारा उद्भूत, निपुणता रूपी खाद द्वारा परिपुष्ट एंव सिंचित तथा अभ्यास रूपी जल द्वारा पुष्पित एंव फलित होकर अपने साहित्य-प्रेमियों को रसास्वादन कराता रहता है।
Comments
Post a Comment